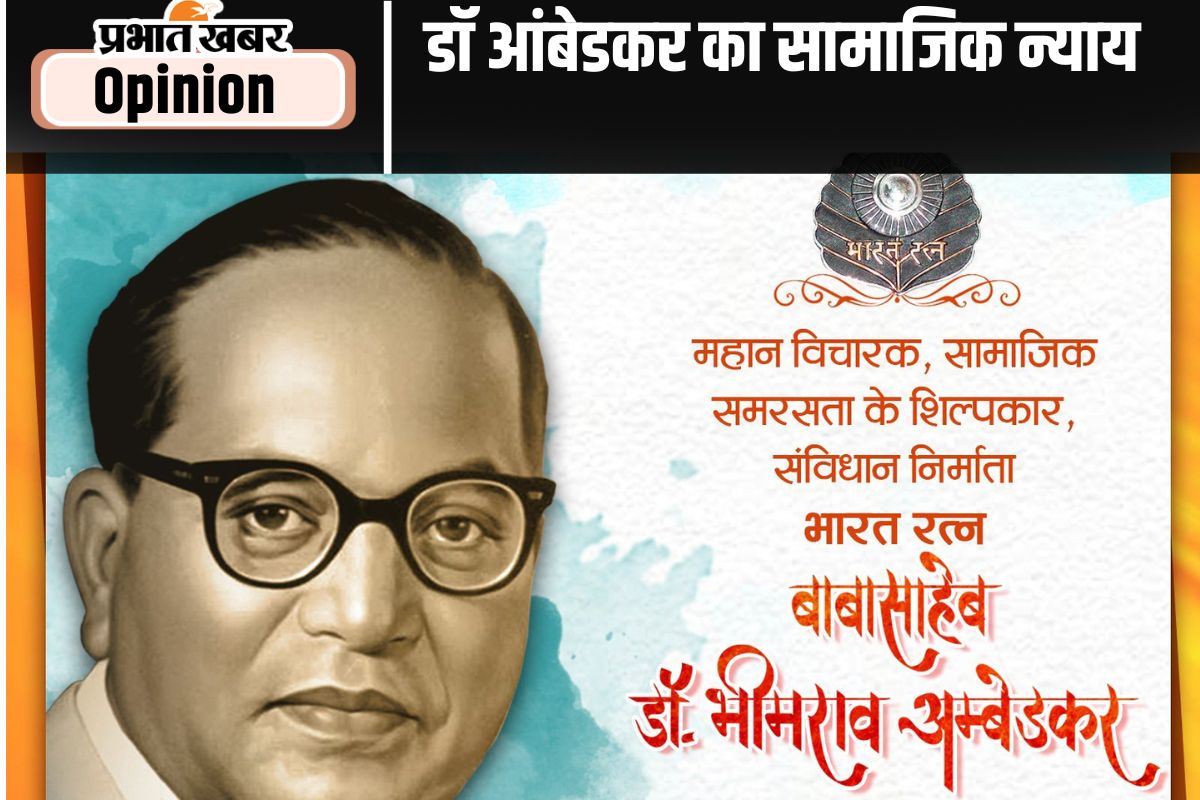–पंकज चौरसिया–
(राजनीतिक विश्लेषक)
BR Ambedkar Jayanti : आज संपूर्ण देश बाबासाहब आंबेडकर को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा है. डॉ आंबेडकर उन विचारकों में से रहे हैं, जिन्होंने लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय और आत्मसम्मान को बढ़ाने का काम किया और जो आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक आधार हैं. आज उनकी विरासत के लिए पहले से कहीं ज्यादा राजनीतिक दावेदार हैं. सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों में उनके विचारों को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करने की होड़-सी लगी है. उनकी विचारधारा को सिर्फ एक चुनावी उपकरण के रूप में उपयोग करने के बजाय इसे वास्तविक सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए.
वर्ष 2014 की चुनावी राजनीति के बाद विभिन्न दल डॉ आंबेडकर की विचारधारा को अपने-अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं. भाजपा उनके राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के विचारों को आगे बढ़ाने का दावा करती है, जबकि कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल उनके सामाजिक न्याय और आरक्षण संबंधी विचारों को प्रमुखता देते हैं. वर्ष 2014 के चुनाव से पहले रिपब्लिकन पार्टी के अलावा डॉ आंबेडकर का स्मरण और विचार अन्य दलों के सीमित प्रचार के लिए ही थे.
डॉ आंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का चुनावी राजनीति पर तो गहरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन राजनीतिक दलों पर आर्थिक न्याय का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है. बाबासाहब का मानना था कि लोगों को केवल संवैधानिक अधिकार देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि चुनावी प्रतिनिधित्व के माध्यम से वंचित वर्गों को शक्ति देना भी आवश्यक है. इसी कारण उन्होंने पृथक निर्वाचिका की मांग की, ताकि दलित वर्गों को वास्तविक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले. हालांकि बाद में यह समझौता उन्हें खेदजनक लगा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह दलितों की असली राजनीतिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व के विचार से समझौता है. बेशक आरक्षण प्रणाली ने विधायिकाओं में दलितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, लेकिन आंबेडकर हमेशा इसके दीर्घकालिक प्रभाव को लेकर संशय में ही रहे.
डॉ आंबेडकर का मानना था कि दलितों को सिर्फ आरक्षित सीट नहीं, समान राजनीतिक अधिकार और स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए. वह इस बात के विरोधी थे कि उच्च जातियों के ‘प्रभुत्व’ से दलितों का उत्थान किया जाए. उन्होंने खुद को और अपनी जाति के लोगों को अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया और इसके लिए आत्मनिर्णय की आवश्यकता को स्वीकार किया. उनका मानना था कि दलितों को खुद को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना होगा. आज चुनावी राजनीति में डॉ आंबेडकर की विचारधारा को दलित, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी राजनीति उनके विचारों को अपने-अपने संदर्भ में ढालकर प्रयोग कर रहे हैं. मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से लेकर और हाल के कुछ वर्षों में ओबीसी और इडब्ल्यूएस आरक्षण पर हो रही चर्चाएं इसी विचारधारा की निरंतरता को दर्शाती हैं.
आज चुनावी राजनीति में सामाजिक न्याय की अवधारणा केवल आरक्षण तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें जातिगत जनगणना, आरक्षण का उपवर्गीकरण, समान प्रतिनिधित्व और निजी सेवाओं में आरक्षण जैसी कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल हो गयी हैं. बाबासाहब सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय की आवश्यकता को समान महत्व देते थे. उनका मानना था कि केवल सामाजिक न्याय की नीतियों से वंचित वर्गों की स्थिति में स्थायी बदलाव नहीं लाया जा सकता, इसके लिए एक समान और समावेशी अर्थव्यवस्था की भी आवश्यकता है. अगर आर्थिक संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाए, तो समाज में वास्तविक बदलाव संभव होगा. उनका उद्देश्य एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना था, जो सामाजिक और आर्थिक न्याय, दोनों को समाहित करे और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए एक सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करे.
आज जब देश की आर्थिक नीति नव-उदारवादी आर्थिक मॉडल पर टिकी हुई है, तब डॉ आंबेडकर की यह सोच काफी भिन्न प्रतीत होती है. आज कई राजनीतिक दलों का ध्यान केवल सत्ता में भागीदारी और आरक्षण प्राप्ति तक सीमित है, जबकि सत्ता में भागीदारी और आरक्षण के माध्यम से केवल आंशिक समस्याओं का समाधान हो सकता है. इसलिए सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले दलों को वंचित समूहों को नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए. वंचित वर्गों की भागीदारी केवल सत्ता तक सीमित न रहे, बल्कि वे नव-उदारवादी आर्थिक मॉडल के भी हिस्से बन पाएं. इस संदर्भ में आंबेडकर के आर्थिक न्याय का दृष्टिकोण बहुत अहम है, क्योंकि वह हमें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मौजूद समस्याओं का समाधान दिखाता है व संस्थाओं को अधिक लोकतांत्रिक बनाने का आग्रह भी करता है.
इसलिए समय-समय पर सामाजिक न्याय की नीतियों में जो कमियां हैं, उन्हें सुधारने के लिए उनमें नये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को समयानुसार शामिल करते रहना चाहिए. इस संदर्भ में आंबेडकर के आर्थिक न्याय का दृष्टिकोण बहुत अहम है, क्योंकि वह हमें सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मौजूद समस्याओं का समाधान दिखाता है. यह आवश्यक है कि नयी सामाजिक न्याय की नीतियों को नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था में विस्तारित किया जाये. इस परिप्रेक्ष्य में, यदि हम वंचित वर्गों के बीच एक प्रभावशाली आर्थिक वर्ग के निर्माण की बात करते हैं, तो यह केवल उनके सामाजिक अधिकारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में भी ठोस कदम होगा. इससे वंचित वर्गों को आर्थिक उद्यमिता के अवसरों, शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों और वित्तीय संसाधनों तक पहुंच के रूप में सशक्त किया जा सकता है. इस तरह की नीतियों से सामाजिक न्याय का मतलब केवल समाज के सबसे निचले वर्गों को सहायताप्रद बनाना नहीं, बल्कि उन्हें सामर्थ्य और आत्मनिर्भरता की दिशा में भी प्रेरित करना होगा. यह दृष्टिकोण न केवल वंचित वर्गों की जीवन स्थितियों में सुधार करेगा, बल्कि समाज की समग्र सामाजिक-आर्थिक संरचना को परिवर्तित करने में भी मदद करेगा.
(ये लेखकद्वय के निजी विचार हैं.)