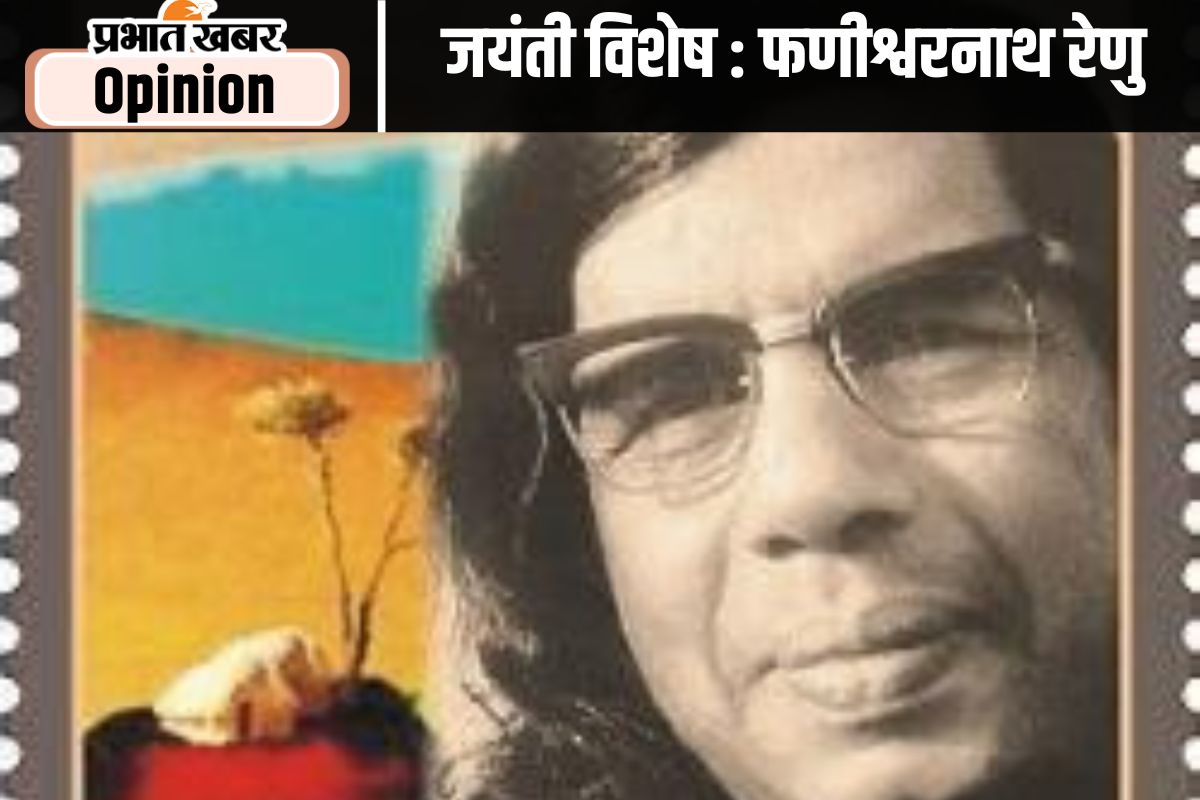Phanishwar Nath Renu : किसी भी रचनात्मक क्षेत्र में अपने समकालीनों के बीच एक प्रतिमान के रूप में प्रतिष्ठित हो पाना दुर्लभ उपलब्धि है. हिंदी के युगांतकारी रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु ने इस दुर्लभ उपलब्धि का वरण किया था. चार मार्च, 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले (अब अररिया) के औराही हिंगना गांव में जन्मे रेणु की इस दुर्लभ उपलब्धि के बारे में जानने के लिए निर्मल वर्मा की इस टिप्पणी से वाकिफ होना जरूरी हो जाता है, ‘मैं जिन लोगों को ध्यान में रखकर लिखता था, उनमें रेणु सबसे प्रमुख थे…. कुछ लोग हमेशा हम पर सेंसर का काम करते हैं, सत्ता का सेंसर नहीं, जिसमें भय और धमकी छिपी रहती है- किंतु एक ऐसा सेंसर, जो हमारी आत्मा और ‘कांशस’, हमारे रचनाकर्म की नैतिकता के साथ जुड़ा होता है. रेणु जी का होना, उनकी उपस्थिति ही एक अंकुश और वरदान थी’. उपरोक्त उद्धरण का महत्व इस बात से और बढ़ जाता है कि इसके उद्गाथा समकालीन हिंदी कथा साहित्य के कद्दावर हस्ताक्षर और विश्व साहित्य के गहना अध्येता निर्मल वर्मा हैं. ऐसे मनीषी व्यक्ति द्वारा देशज अस्मिता के सशक्त पैरोकार रेणु को ‘संत लेखक’ के रूप में याद करना रेणु के सार्वकालिक महत्त्व को उजागर करने के लिए पर्याप्त है.
रेणु शब्द और कर्म की एकता के हामी थे. उन्होंने जो भी लिखा, उसका प्रत्यक्ष जुड़ाव ‘धरतीपुत्रों’ की जीवन स्थितियों, विसंगतियों, संघषों, उल्लासों और प्रमादों से है. रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में रेणु का पदार्पण वर्ष 1944 में महज 23 साल की उम्र में हुआ था. उसी साल उनकी पहली कहानी ‘बटबाबा’ का प्रकाशन कलकत्ता से प्रकाशित विश्वामित्र में हुआ. आज जब पूरी दुनिया में पर्यावरण संकट के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण विमर्श के केंद्र में आ गया है और पाश्चात्य जगत में ‘इको लिटरेचर’ तथा ‘इको क्रिटिसिज्म’ की चर्चा जोरों पर है, तब ‘बटबाबा’ पुनर्पाठ की मांग करती है, क्योंकि इस कहानी का कथ्य भी मूल रूप से पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रित है. इस कहानी का नायक वर्षों पुराना बरगद का एक पेड़ है, जिसे सम्मानपूर्वक ग्रामीण बटबाबा कहते हैं. यह पेड़ जब धीरे-धीरे सूखने लगता है, तब जमींदार जलावन की कमी पूरी करने के लिए इस बटबाबा को काटने का आदेश देता है. इस खबर से पूरे गांव में शोक की लहर फैल जाती है. रेणु ने शोकग्रस्त गांव का दृश्य जिन शब्दों के जरिये खींचा है, उसको पर्यावरण संरक्षण की संवेदनशीलता के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है. इसी क्रम में उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘परती परिकथा’ भी समाहित है जिसमें लेखक ने बंजर धरती को हरित करने के स्वप्न को औपन्यासिक परिधि में मूर्त किया है.
रेणु को सार्वकलिक पहचान देने वाली रचना ‘मैला आंचल’ सिर्फ साहित्यिक नहीं, बल्कि अंतर-अनुशासनिक अध्ययन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक साथ समाज, संस्कृति, राजनीति, इतिहास और आंचलिकता जैसे आयामों को समझने का प्रामाणिक स्रोत है. रेणु ने पूरा जीवन एक एक्टिविस्ट के तौर पर जिया . आजादी का आंदोलन हो या आजादी के बाद अवमूल्यन की पोषक सत्ता संरचना के खिलाफ उपजा जन आंदोलन, रेणु हर जगह जनता के पक्ष में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते रहे. प्रजातांत्रिक समाजवाद के हिमायती रेणु ने कथनी और करनी के हर अंतर को न केवल मिटाया, बल्कि अपनी प्रतिबद्धता को जनपक्षीयता से जोड़कर निर्भीकता का भी परिचय दिया.
आपातकाल के विरोध में पद्मश्री लौटाना इसी निर्भीकता और जनपक्षधरता की बेबाक बानगी है. रेणु हिंदी के एकमात्र ऐसे लेखक हैं, जिन्होंने पड़ोसी देश नेपाल के मुक्ति संघर्ष में – कलम और बंदूक – दोनों के जरिये अपना योगदान दिया. उस परिघटना पर केंद्रित उनकी रचना ‘नेपाली क्रांति कथा’ (रिपोतार्ज) इस जनसंघर्ष की जिंदा गवाही तो है ही, भू-राजनीति के प्रति रेणु की गहरी समझ का भी परिचायक है. ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ जैसा शब्द जब अस्तित्व और प्रचलन से कोसों दूर था, तब पत्रकार रेणु ने समाज को प्रभावित करनेवाली हर घटना को इतनी उत्कृष्टता और सजीवता से शब्दों की चौहद्दी में समायोजित किया कि उनके शब्द कैमरे की तरह सजीव प्रसारण का अनुभव कराते थे.
रेणु के चरित्र श्रमशील समाज के धरतीपुत्र थे. उनकी त्रासदियों और संघर्षो को चित्रित करते हुए लेखक ने समय सापेक्ष विकृतियों, विद्रूपताओं को उभारने के साथ-साथ मानवीयता, सामाजिकता, सामूहिकता को बचाये, बनाये रखने में धरतीपुत्रों की अतुलनीय भूमिका को सदैव पहले पायदान पर जगह दी है . ‘मैला आंचल’ का बावनदास, ‘ठेस’ का सिरचन, ‘संवदिया’ का हरगोबिन, ‘रसूल मिस्त्री’ का रसूल जैसे पात्र ऐसे ही कथा-बिंबों की निर्मिति हैं.
(ये लेखक के निजी विचार हैं.)